देश की आज़ादी के लिए हज़ारों-लाखों लोगों ने लड़ाई लड़ी। हज़ारों ने अपनी जान कुर्बान कर दी लेकिन हम वतन पर मर मिटने वाले कितने लोगों के नाम जानते हैं ? कुछ बड़े क्रांतिकारियों को छोड़ दें तो ज़्यादातर आज़ादी के सिपाही गुमनाम ही रह गए। वो जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश को आज़ाद कराने के लिए न्योछावर कर दिया। ऐसे ही गुमनाम नायकों की दास्तां का दस्तावेज़ीकरण कर रहे हैं शाह आलम राना। आज इंडिया स्टोरी प्रोजेक्ट में कहानी शाह आलम की।
क्रांति की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं
ख़ुद एक क्रांतिकारी परिवार में जन्मे शाह आलम आज ख़ुद भी क्रांति की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, हां उनका अंदाज़ कुछ अलग है। वो उन बिसरी हुई गाथाओं को समेटने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें देश के इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाना चाहिए।
शाह आलम राना मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले के रहने वाले हैं। संत कबीर दास की कर्मभूमि बस्ती। वही बस्ती जिसके बारे में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कभी कहा था- ‘बस्ती को बस्ती कहूं तो काको कहूं उजाड़’। इसी बस्ती के ज़िला मुख्यालय से क़रीब 20 किलोमीटर दूर बसा है पूरा पिरई गांव। इसी गांव के बाशिंदे हैं शाह आलम। माता-पिता खेती करते हैं। तीन भाई-बहनों में सबसे बड़े शाह आलम ने गांव में ही रह कर 12वीं तक की पढ़ाई की फ़िर आगे की पढ़ाई के लिए साल 1999 में अयोध्या चले गए। यहां राम जानकी मंदिर में रहे और डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। उच्च शिक्षा के लिए वो दिल्ली आ गए और जामिया मिल्लिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया।

अयोध्या ने जोड़ा ज़िंदगी का नया अध्याय
अयोध्या ने उनकी ज़िंदगी में ऐसा अध्याय जोड़ दिया जिसने उन्हें एक दिशा दे दी। अयोध्या के राम जानकी मंदिर में रहते हुए शाह आलम का परिचय देश भर में चल रहे छात्र-आंदोलनों से हुआ। इसी दौरान उनका मानवीय और संवैधानिक मूल्यों के प्रति झुकाव बढ़ता गया। सामाजिक सरोकारों के लिए 2002 में चित्रकूट से अयोध्या तक, 2004 में मेंहदीगंज से सिंहचर तक, 2005 में इंडो-पाक पीस मार्च दिल्ली से पाकिस्तान के मुल्तान तक, 2005 में ही सांप्रदायिक सौहार्द के लिए कन्नौज से अयोध्या, 2007 में अयोध्या से मगहर तक कबीर पीस हॉर्मोनी मार्च और 2009 में कोसी से गंगा तक पैदल यात्राएं की।
क्रांतिकारियों की तरफ़ झुकाव
शाह आलम ख़ुद एक ऐसे परिवार से जुड़े हैं जिसने आज़ादी की लड़ाई में अपना बहुत कुछ खोया है। उनके परदादा स्वतंत्रता सेनानी पिरई खां, महुआ डाबर एक्शन के अगुवा रहे थे। 10 जून 1857 को उन्होंने अपने गोरिल्ला साथियों के साथ मिलकर अंग्रेजी सेना के 6 अफ़सरों को मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि इसका ख़ामियाज़ा पूरे परिवार को उठाना पड़ा था, लेकिन आज़ादी के मतवालों को ख़ामियाज़े की फ़िक़्र कहां थी।
शायद यही वजह थी कि शाह आलम भी क्रांतिकारियों पर काम करने लगे। साल 2004 में वो अशोक जतिन के साथ शक्तिपुंज नाम की डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म के काम से जुड़े। लेकिन आने वाले साल उनके लिए और अहम थे।

अयोध्या फ़िल्म फेस्टिवल की शुरुआत
फ़िल्म मेकिंग से जुड़ने के बाद शाह आलम को समझ में आया कि फ़िल्में किसी विषय के डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ही सशक्त ज़रिया हो सकती हैं। इसके बाद उन्होंने साल 2006 में अपने साथियों के साथ मिलकर विरासत नाम का वीडियो म्यूज़िक जारी किया और इसी साल शुरुआत की उत्तर प्रदेश के पहले फ़िल्म फेस्टिवल- अयोध्या फ़िल्म फेस्टिवल की। महान क्रांतिकारी अशफ़ाक-उल्ला-ख़ान और राम प्रसाद बिस्मिल की याद में आयोजित होने वाला अयोध्या फ़िल्म फेस्टिवल आज नए और ऊंचे मक़ाम तक पहुंच चुका है। ‘अवाम का सिनेमा’ के बैनर तले अयोध्या से शुरू हुए सफ़र का अगला ठिकाना मऊ था। मऊ फ़िल्म फेस्टिवल सरदार भगत सिंह की शहादत दिवस से गणेश शंकर विद्यार्थी बलिदान दिवस तक आयोजित किया गया। इसके बाद कारगिल, कैथी, बरहज, जम्मू, जयपुर, आज़मगढ़, बिजनौर, औरैया, कानपुर समेत कई शहरों में फ़िल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस क्रांतिवीरों से जुड़े दस्तावेजों की प्रदर्शनी, फ़िल्में, नाटक और संवाद कार्यक्रमों के ज़रिये नई पीढ़ी तक उनकी महान गाथा और संदेशों को पहुंचाया गया। सबसे बड़ी बात कि इन आयोजनों में शाह आलम ने किसी तरह की सरकारी या प्रायोजकों की मदद नहीं ली। इसका ख़र्च वो ख़ुद और अपने कुछ साथियों के ज़रिये पूरा कर लेते हैं।
आज आयोध्या फ़िल्म फेस्टिवल के आयोजन के 16 साल हो चुके हैं। चौरी-चौरा इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल के 7 और के आसिफ़ चंबल इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल के आयोजन के 6 साल हो चुके हैं। इस दौरान उन्हें कई बार आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा लेकिन शाह आलम रूके नहीं।
काम से मिली पहचान
शाह आलम ने 2009 में लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करने वाले शरीफ़ चाचा पर एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म बनाई जो काफ़ी चर्चा में रही। ख़ास बात ये है कि उनकी ये फ़िल्म पद्मश्री मोहम्मद शरीफ़ के जीवन पर बनी पहली डॉक्टूमेंट्री थी।

चंबल से शाह आलम का प्यार
शाह आलम को चंबल से बहुत प्यार है। चंबल के बीहड़ वाले इलाक़े शाह को अपनी तरफ़ खींचते हैं। उन्होंने साल 2016 में मई, जून और जुलाई के तपते मौसम में अकेले साइकिल चलाकर चंबल के इलाक़े में 2800 किलोमीटर की यात्रा की और बीहड़ का डॉक्यूमेंटेशन किया। ‘चंबल जनसंसद’ और आज़ादी के 70 साल पूरे होने पर ‘आज़ादी की डगर पे पांव’ और 2338 किलोमीटर की यात्रा क्रांतिकारियों के भूलने के विरोध में की। वो ‘मातृवेदी-बागियों की अमरगाथा’, ‘चंबल मेनीफेस्टो’, ‘बीहड़ में साइकिल’, ‘आज़ादी की डगर पे पांव’, ‘कमांडर-इन-चीफ़ गेंदालाल दीक्षित’, ‘बंदूकों का पतझड़’ आदि पुस्तकों के लेखक भी हैं। चंबल संग्रहालय, पंचनद दीप पर्व, चंबल लिटरेरी फेस्टिवल, चंबल मैराथन, चंबल क्रिकेट लीग, चंबल कटहल फेस्टिवल जैसे कई ज़बरदस्त कार्यक्रमों और महोत्सवों के संस्थापक भी हैं।
शाह आलम इन दिनों भी चंबल में ही रह कर चबंल घाटी में आए बदलाव की इबारत लिख रहे हैं। वो जालौन के पास पांच नदियों के संगम के क़रीब चंबल आश्रम में रह रहे हैं। ये चंबल आश्रम कभी कुख़्यात डाकू रह चुके सलीम गुर्जर उर्फ़ पहलवान का है। शाह आलम चाहते हैं कि देश के लिए कुर्बानी देने वाले आज़ादी के हर सिपाही को याद किया जाए। इसके साथ ही चंबल विश्वविद्यालय खोले जाने का सपना भी वो साकार करना चाहते हैं।
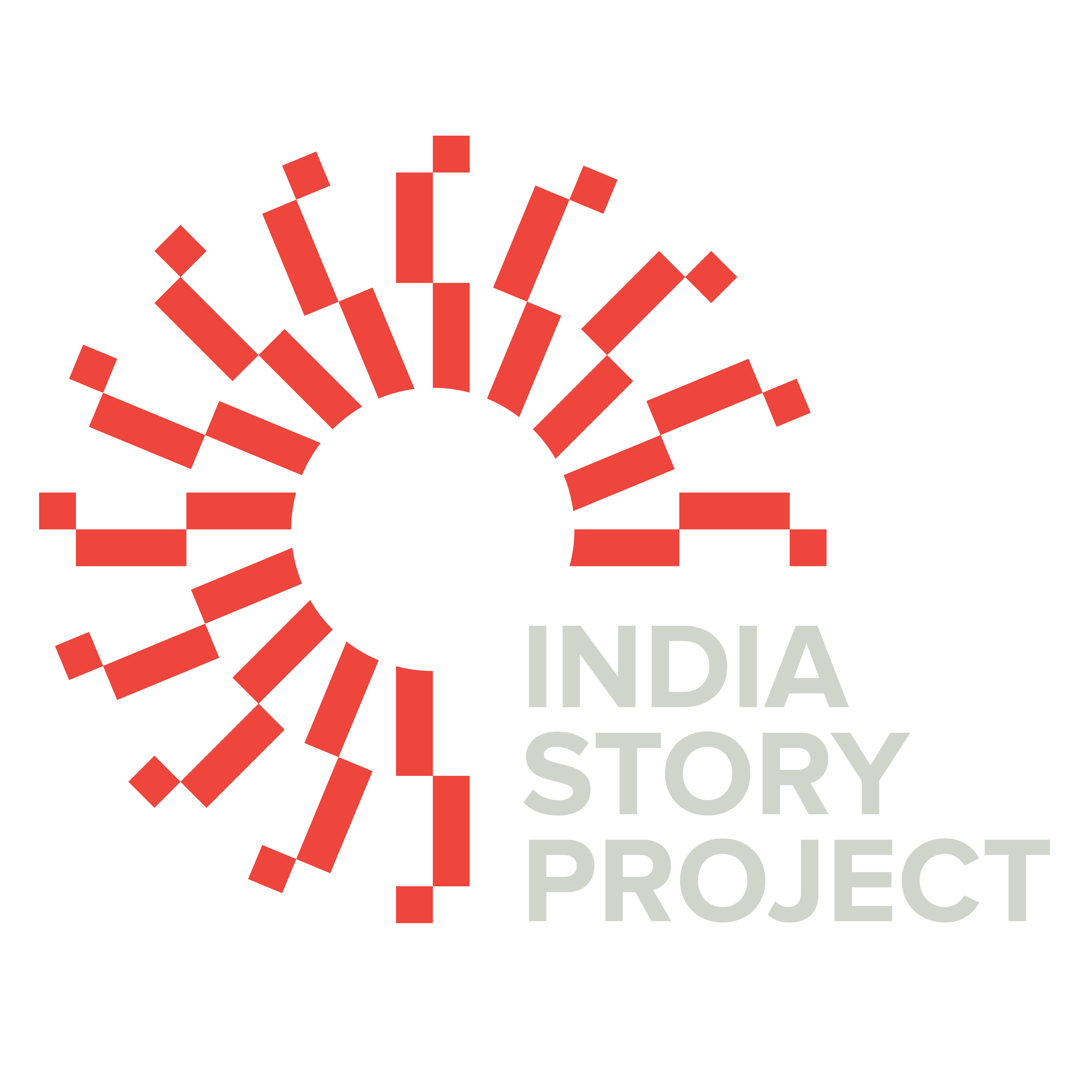




Add Comment